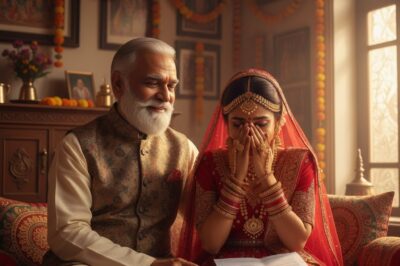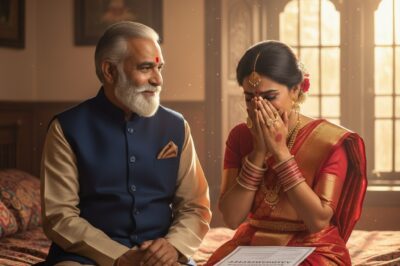वह खरीदारी करने गई और कभी वापस नहीं लौटी—14 साल बाद, परिवार को पता चला दिल दहला देने वाला सच
मुंबई में एक तपती दोपहर थी, ऐसी गर्मी कि हवा शीशे की तरह चमक रही थी।
42 साल की आशा पटेल ने अपने पति और दो बच्चों से कहा कि वह कुछ कपड़े और घरेलू सामान खरीदने क्रॉफर्ड मार्केट जा रही हैं।
आशा को सिलाई का बहुत शौक था। उस सुबह, उसने अपनी छोटी बेटी से वादा किया था कि वह आने वाले दिवाली त्योहार के लिए उसके लिए एक नई ड्रेस बनाएगी।
घर में किसी को नहीं पता था कि यह आखिरी बार होगा जब वे उसे देखेंगे।
उसका पति, रमेश, घर पर टूटे हुए गेट की मरम्मत कर रहा था, जबकि उनके बच्चे—अर्जुन और मीना—घर का काम कर रहे थे।
जैसे-जैसे सूरज ढलने लगा और परछाइयाँ लंबी होने लगीं, आशा अभी भी वापस नहीं लौटी थी।
पहले तो रमेश ने सोचा कि शायद वह किसी दोस्त से मिली होगी या चाय पीने रुकी होगी।
लेकिन रात 9 बजे तक, चिंता होने लगी।
उसने कुछ दुकानों पर फ़ोन किया जहाँ वह अक्सर जाती थी, लेकिन देर दोपहर के बाद से उसे किसी ने नहीं देखा था।
अगली सुबह, वह दादर पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने गया। पुलिसवालों ने नोट लिए, सवाल पूछे और कंधे उचका दिए—कहते हुए कि शायद वह रिश्तेदारों के पास रहने चली गई होगी या तनाव में घर छोड़कर चली गई होगी।
लेकिन रमेश को यह मानने से इनकार था।
“आशा कभी नहीं जाएगी। वह अपने परिवार से प्यार करती है। वह सबसे ज़िम्मेदार इंसान है जिसे मैं जानता हूँ।”
दिन हफ़्तों में बदल गए।
रमेश ने मुंबई के हर अस्पताल, बस अड्डे और रेलवे टर्मिनल की तलाशी ली।
उसने क्रॉफर्ड मार्केट के पास रेहड़ी-पटरी वालों से भी बात की।
कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने उसे कपड़े का एक छोटा सा थैला लेकर बाज़ार से बाहर जाते देखा था, बिल्कुल सामान्य लग रही थी।
और उसके बाद—कुछ नहीं।
हर रात, घर में सन्नाटा छा जाता था।
छोटी मीना अपनी माँ द्वारा छोड़े गए अधूरे कपड़े के टुकड़े को पकड़े हुए रोते-रोते सो जाती थी।
रमेश पिता और माँ दोनों बन गया।
वह खाना बनाता, साफ़-सफ़ाई करता, और चुपचाप अंदर से टूटते हुए परिवार को संभालने की कोशिश करता।
लोग फुसफुसाते थे कि उसे “आगे बढ़ जाना चाहिए”, कि वह शायद हमेशा के लिए चली गई है।
लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका।
उसने उसकी शादी की तस्वीर लिविंग रूम की अलमारी में रख दी – मौत की याद के तौर पर नहीं, बल्कि वापस आने के वादे के तौर पर।
हर दिवाली, वह उसके लिए एक छोटा सा दीया जलाता और अँधेरे में फुसफुसाता:
“आशा, घर आ जाओ। बस एक बार और।”
साल बीतते गए।
बच्चे बड़े हो गए – नाज़ुक बच्चों से मज़बूत जवान वयस्कों में।
अर्जुन ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और अपने पिता की मीना की कॉलेज की फीस भरने में मदद करने के लिए पार्ट-टाइम काम किया।
कभी-कभी, मीना रो पड़ती:
“दूसरी माँएँ स्कूल मीटिंग में क्यों आती हैं… लेकिन मेरी कभी नहीं आती?”
अर्जुन बस उसे चुपचाप गले लगा लेता।
चौदह साल बाद, अर्जुन – जो अब पुणे की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में लॉजिस्टिक्स ऑफिसर है – को पुराने गोदाम के दस्तावेज़ों की जाँच करने का काम सौंपा गया।
धुंधले कागज़ों के ढेर को पलटते हुए, एक नाम सुनकर उसकी धड़कन रुक गई:
“आशा पटेल – अस्थायी निवास परमिट, 2011, घाटकोपर श्रमिक आवास।”
वह स्तब्ध रह गया।
क्या यह सचमुच वही हो सकती है?
उस रात, उसने वह दस्तावेज़ अपने पिता को दिखाया।
रमेश के हाथ काँप रहे थे जब उसने वह दस्तावेज़ पकड़ा।
“वह ज़िंदा थी… इतने सालों से?”
उन्होंने जाँच करने का फैसला किया।
पता उन्हें उस जगह ले गया जहाँ पहले मज़दूरों का आवास हुआ करता था—जो अब ढह गया है।
लेकिन पूर्व केयरटेकर को अब भी वह याद थी।
“हाँ, आशा नाम की एक महिला थी,” उसने कहा। “वह पास की एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करती थी। वह शांत और दयालु थी… लेकिन कभी-कभी वह भ्रमित लगती थी। एक दिन, काम पर उसकी तबियत बिगड़ गई, और कुछ लोग उसे अस्पताल ले गए। वह कभी वापस नहीं आई।”
रमेश और अर्जुन ने एक-दूसरे को देखा—उम्मीद और डर का मिश्रण।
वे ठाणे के एक मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल पहुँचे, जो नीम के पेड़ों से घिरा एक शांत अस्पताल था।
जब उन्होंने उसका नाम लिया, तो एक नर्स की आँखें चौड़ी हो गईं।
“आशा पटेल? हाँ… वह कई सालों से यहाँ है।”
नर्स उन्हें एक लंबे गलियारे से होते हुए एक छोटे से वार्ड में ले गई।
वहाँ, खिड़की के पास, एक दुबली-पतली औरत बैठी थी जिसके छोटे-छोटे भूरे बाल थे।
वह बाहर देख रही थी, विचारों में खोई हुई, धूप उसके नाज़ुक कंधों पर पड़ रही थी।
जब रमेश फुसफुसाया,
“आशा…”
उसने धीरे से अपना सिर घुमाया।
उसकी आँखें पहले उलझन से झपक उठीं – फिर पहचान गईं।
“रमेश? क्या यह… सच में तुम हो?”
रमेश घुटनों के बल गिर पड़ा, उसके चेहरे पर आँसू बह रहे थे।
चौदह साल।
चौदह लंबे, खाली साल – और वह हमेशा से ज़िंदा थी।
डॉक्टरों ने बताया कि आशा को एक दशक से भी पहले हल्के स्ट्रोक और अस्थायी भूलने की बीमारी के बाद अस्पताल लाया गया था।
उसे अपना नाम, पता या परिवार याद नहीं आ रहा था।
जब कोई उसे लेने नहीं आया, तो उसे मनोरोग वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया।
बाद में उसे हल्का सिज़ोफ्रेनिया और अवसाद हो गया – वह चुपचाप रह रही थी, दुनिया से भुला दी गई थी।
रमेश चुपचाप सुन रहा था, उसका दिल एक साथ टूट रहा था और भर रहा था।
वर्षों का दुःख, क्रोध और अनुत्तरित प्रश्न आंसुओं में घुल गए
परिवार हर हफ़्ते उससे मिलने आता था।
वे उसके लिए उसकी पसंदीदा मिठाइयाँ—जलेबी और पोहा—लाते थे ताकि घर की यादें ताज़ा हो जाएँ।
वे उसे पुराने दिनों की कहानियाँ सुनाते थे—अर्जुन के स्कूल की, मीना की शादी की पोशाक की, जो वह कभी नहीं सिल पाई।
कभी-कभी उसे याद आता था।
वह मंद-मंद मुस्कुराती और फुसफुसाती,
“मीना का एक जोड़ा मुझे अब भी देना है…”
और दिन, वह चुपचाप बैठी रहती, अतीत और वर्तमान के बीच खोई हुई।
लेकिन किसी को परवाह नहीं थी।
वह घर पर थी—और बस इतना ही काफी था।
अर्जुन ने एक शाम अपने पिता को गले लगाया और धीरे से कहा:
“कम से कम अब हमें पता तो चला, पापा। हमने उसे ढूंढ लिया। बस यही मायने रखता है।”
मीना, जो अब 20 साल की है, अपनी माँ का हाथ पकड़कर रो पड़ी,
“माँ, मैंने पूरी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार किया है।”
आशा मंद-मंद मुस्कुराई और फुसफुसाई,
“और मैं… तुम्हें भी ढूँढने का इंतज़ार कर रही थी।”
पटेल परिवार के घर में धीरे-धीरे ज़िंदगी रंग भरने लगी।
दर्द गायब नहीं हुआ – बस कृतज्ञता में बदल गया।
चौदह साल के नुकसान ने उन्हें एक अनमोल बात सिखा दी थी:
प्यार गायब नहीं होता। यह इंतज़ार करता है।
तब से हर दिवाली पर, परिवार चार दीये जलाता है – एक उन दोनों के लिए, और एक उस चमत्कार के लिए जिसने उन्हें फिर से एक साथ ला दिया।
और जैसे ही लौ धीरे-धीरे टिमटिमाती है, रमेश हमेशा फुसफुसाता है,
“कुछ सफ़र सालों में बीत जाते हैं… लेकिन प्यार हमेशा अपना रास्ता ढूँढ ही लेता है।”
“भारत में, वे कहते हैं: ‘रिश्तों का बंधन कभी टूटता नहीं – वक़्त बस उसे परख लेता है।’
और पटेल परिवार के लिए,
चौदह साल का इंतज़ार त्रासदी में नहीं –
बल्कि पुनर्मिलन के शांत चमत्कार में समाप्त हुआ,
इस बात का प्रमाण कि सबसे लंबी खामोशी के बाद भी,
प्यार घर वापसी का रास्ता याद रखता है।
मुंबई में मानसून आ गया था –
पहले हल्का, फिर तेज़ और बेरहम।
अस्पताल की खिड़की पर पड़ती बारिश की हर बूँद आशा पटेल के खोए हुए सालों की याद दिला रही थी – चौदह लंबे, अकेले साल जो यादों की दरारों से चुपचाप फिसल रहे थे।
ठाणे के मनोरोग वार्ड में,
वह हर दिन उसी खिड़की के पास बैठती,
बारिश की बूंदों को शीशे से नीचे गिरते देखती,
मानो आसमान ही उसकी भूली हुई ज़िंदगी के लिए रो रहा हो।
लेकिन इस बार, वह अकेली नहीं थी।
हर सुबह, रमेश उसके पसंदीदा खाने का टिफिन लेकर आता –
दाल, चावल और आम के अचार का एक छोटा सा टुकड़ा।
अर्जुन उसके बिस्तर के पास ताज़े फूल लाता,
और मीना, जो अब बड़ी हो चुकी है, अपनी माँ के बाल बनाती –
ठीक वैसे ही जैसे आशा बचपन में अपने बाल बनाती थी।
इसकी शुरुआत किसी छोटी सी बात से होती थी।
एक दोपहर, जब मीना ज़मीन पर बैठकर फटे तकिये का कवर सिल रही थी, आशा ने उसके हाथों की ओर देखा—जिस तरह उसकी उंगलियाँ तेज़ी और कोमलता से हिल रही थीं—और फुसफुसाई:
“तुम सिलाई करती हो… बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं करती थी।”
मीना ठिठक गई, उसकी आँखों में आँसू भर आए।
“हाँ, माँ। तुमने मुझे सिखाया था… याद है?”
आशा ने पलकें झपकाईं, उसकी नज़र दूर तक भटक गई।
फिर उसने धीरे से कहा,
“मैं सिलाई कर रही थी… एक नीली ड्रेस। किसी के लिए।”
चौदह सालों में पहली बार उसे कुछ खास याद आया था।
डॉक्टरों ने इसे “एक चिंगारी” कहा।
यादों की एक नाज़ुक लौ जिसे सावधानीपूर्वक पोषित करने की ज़रूरत थी।
उस दिन से, परिवार ने उसकी दुनिया को फिर से बनाने का अपना मिशन बना लिया—एक-एक याद।
रमेश पुराने खत ज़ोर से पढ़ता,
उसकी आवाज़ काँपती हुई लेकिन धैर्यवान।
“आशा, तुम हर चीज़ के लिए सूचियाँ लिखती थीं। यहाँ तक कि किराने की खरीदारी के लिए भी। तुमने कहा था कि इससे तुम्हें शांत रहने में मदद मिलती है।”
अर्जुन ने उसे तस्वीरें दिखाईं—समय के साथ धुंधली होती जा रही श्वेत-श्याम—जब वह उसे गोद में लिए हुए थी।
“यह मैं हूँ, माँ। आपका बेटा। आपने स्कूल का एक भी कार्यक्रम नहीं छोड़ा।”
और मीना उसके लिए कपड़े का वह अधूरा टुकड़ा ले आई जो आशा उस दिन छोड़ गई थी जब वह गायब हुई थी—वही कपड़ा जो उसकी दिवाली की पोशाक बनने वाला था।
जब आशा ने उसे छुआ, तो उसकी उंगलियाँ काँप उठीं।
उसने आँखें बंद कीं और फुसफुसाया:
“मीना… मैंने तुमसे एक पोशाक का वादा किया था, है ना?”
उस रात, एक दशक से भी ज़्यादा समय में पहली बार, आशा नींद में मुस्कुराई।
हफ़्ते बीत गए।
फिर एक बरसाती शाम, एक नर्स ने आशा को खिड़की के पास खड़े होकर धीरे से गुनगुनाते हुए पाया।
एक धुन—पुरानी, धीमी—लेकिन जानी-पहचानी।
अगली सुबह जब रमेश आया, तो उसने उसकी तरफ देखा और कहा:
“तुम हमेशा फ़ैक्टरी से देर से घर आते थे। मैं तुम्हें रात का खाना भूल जाने के लिए डाँटती थी।”
वह स्तब्ध रह गया।
“आशा… तुम्हें याद है?”
उसने धीरे से सिर हिलाया, उसके गालों पर आँसू बह रहे थे।
“और अर्जुन अपना होमवर्क बिस्तर के नीचे छिपा देता था।
और मीना… उसे दिवाली पर एक नीली ड्रेस चाहिए थी।”
रमेश रो पड़ा, उसके बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गया।
चौदह साल का इंतज़ार उस एक पल में सिमट गया –
आँसुओं, हँसी और अविश्वास का सैलाब।
आशा ने हाथ बढ़ाया और अपने नाज़ुक हाथों में उसका चेहरा थाम लिया।
“तुमने मेरा इंतज़ार किया?”
“हमेशा,” उसने फुसफुसाया। “हर दिन।”
महीनों बाद, आशा को छुट्टी मिल गई।
परिवार उसे पुणे स्थित अपने छोटे से अपार्टमेंट में ले आया, जो नए रंग-रोगन से चमक रहा था और गेंदे के फूलों से चमक रहा था।
पड़ोसी उसका स्वागत करने के लिए बाहर इकट्ठा हुए – जो महिलाएँ कभी गपशप करती थीं, अब गले लगकर और मिठाइयाँ देकर खुशियाँ मना रही थीं।
अर्जुन ने उसके लिए एक छोटा सा सिलाई कक्ष बनवाया था, जिसकी खिड़की पूर्व दिशा में थी।
वापस आने वाली पहली सुबह, सूरज की रोशनी उसकी सिलाई मशीन पर पड़ रही थी – पुरानी, जंग लगी, लेकिन अभी भी काम कर रही थी।
उसने उस पर अपनी उंगलियाँ फिराईं और फुसफुसाया,
“मेरे पुराने दोस्त…”
रमेश मुस्कुराया।
“हमने इसे कभी फेंका नहीं। हम इंतज़ार कर रहे थे कि तुम इसे दोबारा इस्तेमाल करो।”
उस दिन, आशा ने फिर से सिलाई शुरू कर दी – सिर्फ़ कपड़ा ही नहीं,
बल्कि अपनी ज़िंदगी के टूटे हुए धागे भी।
अर्जुन एक मज़बूत और ज़िम्मेदार इंसान बन गया था –
लेकिन अपनी माँ को पाने के बाद, उसने नरम होना सीखा।
उसके अंदर बरसों से जमा कठोरता पिघल गई।
उसने गुमशुदा लोगों के एक केंद्र में स्वयंसेवा करना शुरू कर दिया,
और दूसरे परिवारों को उनके प्रियजनों से मिलाने में मदद करने लगा।
मीना, जो कभी शांत और डरी हुई थी, एक कलाकार बन गई।
उसने खिड़कियों के पास इंतज़ार करती महिलाओं के चित्र बनाने शुरू किए,
कोमल आँखों वाली महिलाएँ जो प्यार और समय का भार ढो रही थीं।
जब उससे पूछा गया कि उसने उन्हें क्यों बनाया, तो उसने कहा:
“क्योंकि मेरी माँ हमारा इंतज़ार करती थीं, तब भी जब उन्हें याद नहीं रहता था कि हम कौन हैं।”
एक शाम, जब दिवाली नज़दीक आ रही थी, मीना अपनी माँ के सिलाई वाले कमरे में दाखिल हुई।
सिलाई मशीन की आवाज़ हवा में गूंज रही थी।
आशा ने ऊपर देखा, धीरे से मुस्कुराई।
“मैंने इसे पूरा कर लिया।”
उसने एक खूबसूरत नीली पोशाक दिखाई, जिसकी कढ़ाई लैंप के नीचे नाज़ुक और चमक रही थी।
मीना ने सदमे से अपना मुँह ढक लिया।
“माँ… वही जिसका वादा तुमने मुझसे छह साल की उम्र में किया था।”
आशा की आँखें नम हो गईं।
“मैंने भले ही चौदह साल गँवा दिए हों… लेकिन मैं कभी नहीं भूली कि प्यार कैसा होता है।”
वे गले मिले –
भाग्य से बिछड़ी माँ और बेटी,
अब क्षमा और विश्वास से फिर से मिल गईं।
बाहर, आसमान में पटाखे फूट रहे थे,
उनकी रोशनी आशा की नम आँखों में झलक रही थी।
“देवताओं ने मेरी याददाश्त छीन ली,” उसने फुसफुसाते हुए कहा,
“लेकिन उन्होंने मुझे मेरा परिवार वापस दे दिया।”
गायब होने के बाद अपनी पंद्रहवीं दिवाली पर, आशा छोटे से पारिवारिक वेदी के सामने खड़ी थी।
उसने चार दीये जलाए – एक अपने लिए, एक रमेश के लिए, एक अर्जुन के लिए, और एक मीना के लिए।
उसके हाथ अब नहीं काँप रहे थे।
उसका मन साफ़ था।
उसे सब कुछ याद था – बाज़ार, बेहोशी का दौरा, खोए हुए साल।
लेकिन वह रोई नहीं।
इसके बजाय, वह मुस्कुराई और कृतज्ञता की प्रार्थना फुसफुसाई:
“मुझे घर लाने के लिए शुक्रिया… भले ही इसमें मेरी आधी ज़िंदगी लग गई हो।”
रमेश उसके पीछे आया और उसके कंधों पर गेंदे के फूलों की माला डाल दी।
“आशा, तुम हमारे दिलों से कभी नहीं गईं। यही मायने रखता है।”
परिवार दीयों की सुनहरी चमक में नहाया हुआ एक साथ खड़ा था।
किसी शब्द की ज़रूरत नहीं थी – बस शांति।
“भारत में, वे कहते हैं:
‘याद चली जाए तो भी प्यार नहीं जाता।’
क्योंकि अंत में, यादें भूल सकती हैं –
लेकिन दिल हमेशा याद रखता है।
और आशा पटेल की कहानी – वह महिला जो खामोशी में खो गई और प्यार के ज़रिए लौट आई –
मुंबई की गलियों में फुसफुसाती एक कहानी बन गई:
“जब प्यार सच्चा होता है, तो समय भी उसे मिटा नहीं सकता।”
News
न्यू दिल्ली टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर हाथ में लिए, मैं रो पड़ी क्योंकि मेरी फॉस्टर मां ने मुझे स्कूल छुड़वाकर गांव के 60 साल के मिस्टर शर्मा से शादी करने पर मजबूर किया, ताकि मेरे छोटे भाई को मेरठ में मेडिकल स्कूल में पढ़ने के लिए दहेज के पैसे मिल सकें। मेरी शादी के दिन, पूरे गांव ने मुझ पर उंगली उठाई और गॉसिप की, तरह-तरह की बुरी बातें कहीं। मेरी शादी की रात, मेरे पति अंदर आए और बिस्तर पर दो चीजें रख दीं जिससे मैं चुपचाप रो पड़ी…
जिस दिन मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिला, मैं रोई नहीं। मैं बस घर के पीछे कुएं के पास काफी देर तक…
इतने सालों तक तुम्हें पालने के बाद, अब समय आ गया है कि तुम अपनी माँ की मेहरबानी का बदला चुकाओ!/hi
न्यू दिल्ली टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर हाथ में लिए, मैं रो पड़ी क्योंकि मेरी फॉस्टर मां ने मुझे…
अपनी पत्नी को छोड़कर डायरेक्टर की बेटी से शादी करने की खुशी में मैं बहुत खुश था, लेकिन शादी की रात जब उसने अपनी ड्रेस उठाई तो मैं हैरान रह गया।/hi
अपनी पत्नी को छोड़कर डायरेक्टर की बेटी से शादी करने की खुशी में, मैं अपनी शादी की रात हैरान रह…
कंपनी में एक खूबसूरत शादीशुदा औरत को पटाने पर गर्व करते हुए, मैं आज सुबह उठा और जब मैंने अपनी तरफ देखा तो हैरान रह गया।/hi
काम की जगह पर एक खूबसूरत शादीशुदा औरत को जीतने पर गर्व महसूस करते हुए, मैं एक सुबह उठा और…
आधी रात को, मेरी हॉट पड़ोसन मेरे दरवाज़े पर दस्तक देकर अंदर आने के लिए कहने लगी, और जब मुझे उसकी हरकतों के पीछे का असली मकसद पता चला तो मैं हैरान रह गई…/hi
आधी रात को, मेरी हॉट पड़ोसन ने अंदर आने के लिए मेरा दरवाज़ा खटखटाया, और जब मुझे उसकी हरकतों के…
मेरे बेटे ने गांव वाला अपना घर बेच दिया, अपने माता-पिता की सारी सेविंग्स—4 करोड़ रुपये—इकट्ठी कीं और शहर में एक घर खरीदा। लेकिन फिर वह अपनी पत्नी के माता-पिता को अपने साथ रहने के लिए ले आया, जबकि वे मेरी पत्नी और मेरे साथ, जो गांव में रहते थे, ऐसा बर्ताव करते थे जैसे हमारा कोई वजूद ही न हो। गुस्से में, मैं बिना बताए डिनर के समय उनसे मिलने चला गया। मेरे बेटे ने जवाब दिया, “तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ रही हो?” और उसके बाद मेरी बहू ने जो किया, उससे मैं हैरान रह गया।/hi
मेरे बेटे ने गांव में हमारा घर बेच दिया, अपने माता-पिता की सारी सेविंग्स—4 करोड़ रुपये—इकट्ठी कीं और शहर में…
End of content
No more pages to load